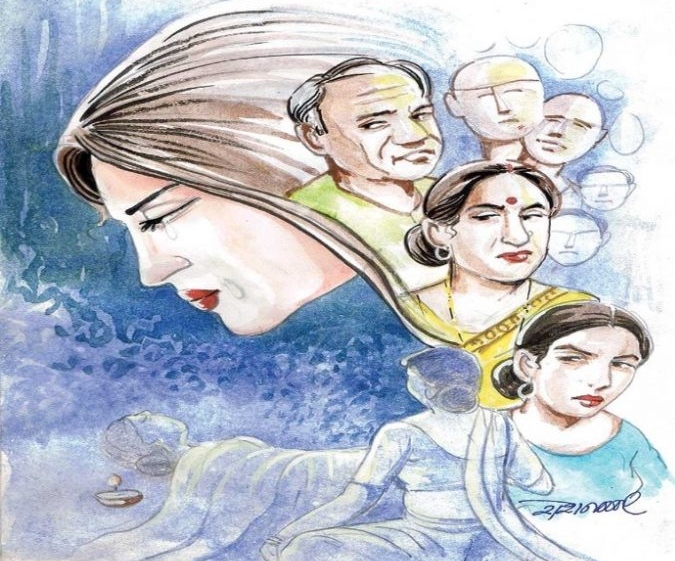“तुम कहती थी मां कि बेटियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगी, तो उन्हें पराश्रित का जीवन नहीं जीना पड़ेगा. अपनी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत के लिए पति के आगे हाथ नहीं पसारने होंगे. आत्मनिर्भर तो हो गईं वे, पर अब तो उन्हें दो मोर्चों पर एक संग जूझना पड़ रहा है मां. पहले जब वह सिर्फ़ घर और बच्चे संभालती थी, तब की बात और थी, परंतु अब भी भले ही वह पति की तरह पूरा दिन नौकरी करके, थककर घर लौटे, घर और बच्चे संभालना आज भी पत्नी का ही दायित्व है. मुश्किल यह है कि हमने अपनी बेटियों को तो मज़बूत बना दिया, पर अपने बेटों की सोच नहीं बदली..."
आज उस कमरे की खिड़की पर पर्दा ड़ा है, पर घर का मुख्यद्वार खुला है. द्वार के पास कतार से जूते लगे हैं. मैं जूते उतारकर चुपचाप भीतर चली गई हूं. मां अपने सारे कर्त्तव्य पूरे कर, सब चिंताओं से मुक्त हो आंखें मूंदें सो गई हैं- सदैव के लिए. भइया अभी पहुंचे नहीं हैं. अब कल ही होगा दाह संस्कार. दीदी और मैं आज की रात बारी-बारी से मां के पास बैठेंगे. पापा बेचैनी के साथ अंदर-बाहर हो रहे हैं. ऑटोवाले को पूरे पैसे पकड़ा मैं नीचे उतरी और कुछ देर वहीं खड़ी रही. सामने घर को यूं देखा जैसे पहली बार देख रही हूं, जबकि जीवन के 24 वर्ष यहीं गुज़ारे हैं. हज़ारों बार गुज़री हूं इस सड़क से. नज़रें स्वयं खिड़की की तरफ़ उठ गईं. कहीं भीतर आशा बची रह गई थी कि क्या मां आज भी उस खिड़की पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी?
मुझे देख जल्दी से किवाड़ खोल कहेंगी, “आज भी इतनी देर कर दी मन्नु.” डांट नहीं, गिला नहीं. बस चिंता से भीगा एक वाक्य.
“हॉस्पिटल की ड्यूटी में देर हो ही जाती है मां. बीमार को यूं तो नहीं कह सकते न कि मेरी ड्यूटी का समय ख़त्म हुआ, मैं जा रही हूं. जब तक मेरी जगह लेनेवाली दूसरी डॉक्टर न आ जाए और मैं उसे मरीज़ों के विषय में पूरी रिपोर्ट न दे दूं. मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती.” मैं मां को समझाती, पर मां शिकायत तो कर ही नहीं रहीं, चिंता व्यक्त कर रही हैं.
अंधेरा घिरते ही वे खिड़की पर आकर खड़ी हो जाती हैं. पम्मी दीदी के विवाह के बाद से तो वह और भी पज़ेसिव हो गई हैं. ज़रा-सी देर होने पर ही घबरा जाती हैं. बाद में मैंने खिड़की के पास एक कुर्सी रख दी, ताकि कम से कम खड़ी तो न रहें. आज उस कमरे की खिड़की पर पर्दा पड़ा है, पर घर का मुख्यद्वार खुला है. द्वार के पास कतार से जूते लगे हैं. मैं जूते उतारकर चुपचाप भीतर चली गई हूं. मां अपने सारे कर्त्तव्य पूरे कर, सब चिंताओं से मुक्त हो आंखें मूंदें सो गई हैं- सदैव के लिए.
भइया अभी पहुंचे नहीं हैं. अब कल ही होगा दाह संस्कार. दीदी और मैं आज की रात बारी-बारी से मां के पास बैठेंगे. पापा बेचैनी के साथ अंदर-बाहर हो रहे हैं. अभी तक पम्मी दीदी ने ही पापा का हाथ बंटाया है मां की देखभाल के लिए. मैं कुछ भी नहीं कर पाई. शहर में होते हुए भी मां-पापा के काम न आ सकी. घर की ज़िम्मेदारियों से भी बोझिल होता है उन्हें बोझ की तरह ढोने को बाध्य होना, वरना दीदी की ज़िम्मेदारियां मुझ से कम हैं क्या? अथवा वह अपने उत्तरदायित्व नहीं निभातीं?
अपने उत्तरदायित्व तो मां ने भी पूरे निभाए थे. सिर्फ़ हम भाई-बहनों के प्रति ही नहीं, बल्कि संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति. दादा-दादी की बीमारी में उनकी अच्छी तरह तीमारदारी तो की ही, ताऊजी का भी यहां लाकर जब ऑपरेशन करवाया गया, तब ढाई महीने तक तीन जन रुके हमारे घर. तब मां ने पूरे मन से की उनकी देखभाल. फिर भी पापा से तमाम उम्र उलाहने ही सुनती रहीं. कभी काम में मीनमेख, कभी ख़र्च के लिए डांट. ऐसा नहीं कि पापा की आय कम थी, पर उनके हिसाब से वे कमाते थे, इसलिए स़िर्फ उन्हीं का अधिकार है उनकी आय पर और उनकी इजाज़त के बिना कोई एक पाई भी ख़र्च नहीं कर सकता था.
मां की ज़रूरतें पूरी करना भी उनके कर्त्तव्य क्षेत्र में नहीं आता था. तीज-त्योहार में जो आ जाता, उसी से काम चलातीं वे, पर जूता-चप्पल ख़रीदने पर भी पहले उन्हें पापा का लंबा-चौड़ा व्याख्यान सुनना पड़ता था.
“तुम इतनी जल्दी चप्पल तोड़ देती हो, इस साड़ी का रंग ही तो ख़राब हुआ है. घर में पहनने में क्या बुराई है?” शादी-ब्याह में जाते वक़्त उनके पास ढंग की साड़ी न होती और वह कोई प्रिंट साड़ी पहन के जातीं, तो मुझे बहुत बुरा लगता. पापा इधर-उधर दौरे पर जाते, तो अपने लिए कपड़े ख़रीद लाते, क्योंकि उनके अनुसार दफ़्तर में पहनने के लिए ढंग के कपड़े होने ही चाहिए. उनको इस बात का भी मलाल था कि मां पैंट-शर्ट क्यों नहीं पहनती थीं, ताकि उनके पुराने पड़ गए कपड़े मां घर पर पहन लें. वो मां, जिनसे बड़ों के सामने सिर ढंककर रहने की उम्मीद की जाती थी.
शौक रखने के बारे में तो मां ने कभी सोचा भी न होगा, जब ज़रूरतें ही पूरी न कर पाती थीं. हर चीज़ के लिए मन मसोसकर रह जाती थीं वे. तमाम उम्र निर्भरता का जीवन जीया उन्होंने. अत: बेटियों को पढ़ाना उनके जीवन का ध्येय बन गया. ‘आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी उनकी बेटियां.’ उन्होंने दृढ़ निश्चय किया. यही कारण था कि वह हम दोनों बहनों को पढ़ने के लिए ख़ूब प्रेरित करती थीं.
“जो चाहो वही लाइन चुनो, पर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ. मुझे तुम्हारे भाई की इतनी चिंता नहीं. उसका करियर तो बन ही जाएगा. पढ़ाई में तेज़ न होगा, तो पापा उसे कोई व्यापार शुरू करवा देंगे. मुझे तुम दोनों की फ़िक्र है. तुमने पढ़ाई में ज़रा ढील दी कि पापा तुम्हारा विवाह कर कर्त्तव्य मुक्त हो जाएंगे.”
दीदी को बचपन से ही अध्यापिका बनने का शौक था. आसपास के छोटे बच्चों को इकट्ठा कर और मां का दुपट्टा साड़ी की तरह लपेट उन्हें पढ़ाने का अभिनय करतीं. कभी बच्चे न जुटते, तो अपने गुड्डे-गुड़ियों एवं अन्य खिलौनों को पंक्तिबद्ध बिठाकर पढ़ाने लगतीं. मुझसे तीन वर्ष बड़ी थीं, मुझे तो वास्तव में ही होमवर्क इत्यादि में सहायता करतीं.
यूं तो मां भी बीए पास थीं और बचपन में हमें वही पढ़ाती थीं, किन्तु आजकल के विषय यथा कंप्यूटर और विज्ञान में दीदी ही सहायता करती थीं. दीदी ने एमएससी करने के पश्चात बीएड किया और एक अच्छे से स्कूल में नौकरी भी करने लगीं. मां संतुष्ट थीं कि जैसा चाहा वैसा ही हुआ सब. दीदी विवाह पश्चात भी अपनी नौकरी क़ायम रखे थीं. मेरा ध्येय डॉक्टर बनने का था. प्रारंभ से ही मेरी विज्ञान में रुचि थी. मेहनत की और मेडिकल में दाख़िला भी पा गई. एमडी के अंतिम वर्ष में मेरा विवाह डॉ. रमन के साथ हो गया. यह तो बाद में पता चला कि उनके लिए विवाह का अर्थ कोई नेह बंधन नहीं, तौलकर की हुई तिज़ारत थी. रमन के पिता ने अपनी अति साधारण-सी नौकरी से बेटे को मेडिकल तो करवा दिया था, अब अपना एक नर्सिंग होम बनाना पिता-पुत्र का सपना था. लेकिन पूंजी का सख़्त अभाव था.
दो कमरों का एक छोटा-सा फ्लैट, वह भी किराए का. एक कमरे में रमन के मम्मी-डैडी, एक में हम. मैं तो इससे भी तृप्त थी, परंतु इसमें उस सपने को पूरा करने की गुंजाइश नहीं थी. उसी योजना का हिस्सा था- एक डॉक्टर लड़की से विवाह करना. इसमें एक लाभ बाद में एक डॉक्टर का वेतन बच जाने का भी था.
एमडी समाप्त होते ही मुझे उसी अस्पताल में नौकरी भी मिल गई. स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के कारण मुझे कई बार लौटने में देर हो जाती और कभी असमय भी जाना पड़ जाता. उस पर रमन के डैडी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, “अस्पताल में भले ही तुम डॉक्टर हो, पर घर में बहू बनकर रहना होगा.” अर्थात् रसोई संभालना एवं भाग-भागकर सब की फ़रमाइशें पूरी करना मेरा कर्त्तव्य था. उस पर मम्मीजी का कहना था कि मेडिकल की लंबी पढ़ाई में उम्र यूं ही आगे खिसक जाती है, अत: बच्चे का जन्म अब और टाला नहीं जा सकता. सो एमडी पूरी करते ही यह मांग भी पूरी कर दी. पांच माह की छुट्टी तो मिल गई, किन्तु उसके बाद काम पर जाना शुरू करना ही था.
बड़े-बड़े सपनों के बीच आया रखने की गुंजाइश नहीं थी. अस्पताल से लौटती, तो मुन्ने को पकड़ाकर मम्मीजी कहतीं, “लो संभालो इसे.” और जाकर लेट जातीं. कपड़े बदलने तक का समय न मिलता मुझे. मुन्ना तो दोपहर में अपनी नींद पूरी कर चुका होता. रसोई में ही उसे झूले में लिटा सब को चाय देती, स्वयं वहीं खड़े-खड़े पीकर रात के भोजन की तैयारी में जुट जाती.
इमर्जेंसीवाले दिन प्रायः देर हो जाती, तो ताना सुनने को मिलता, “कहां लगा दी इतनी देर? मुन्ने ने थका दिया है.” पैसा कमाने की मशीन बन गई मैं. तबीयत ख़राब होने पर सहानुभूति की बजाय क्रोध दर्शाया जाता. बुरा तब लगता, जब रमन भी वही रवैया अपनाते. मुन्ना मुझ अकेले का तो नहीं, उसे ही संभाल लेते, तो भी थोड़ी राहत मिलती. कभी मैं उनके हाथ में ज़बर्दस्ती दे भी देती, तो यह कहकर तुरंत लौटा देते, “यह काम मेरे बस का नहीं.” मैंने अनेक बार प्यार से समझाने की कोशिश की, परंतु कुछ असर नहीं पड़ा.
कभी सहायता का हाथ बढ़ाते भी तो डैडीजी टोक देते, “क्या महिलाओंवाले काम कर रहे हो?” मम्मी-डैडी तो चलो पुराने विचारवाले थे, परंतु रमन को तो उन्हें समझाना चाहिए था कि जब मैं कमाने में उनका पूरा साथ दे रही हूं, तो घर संभालने में उन्हें भी मेरा साथ देना चाहिए था. बेटा दो वर्ष का हो चुका है. एक बार सोचा कि उसे घर पर ही छोड़ जाऊं. शोकवाले घर में परेशान हो जाएगा, पर कोई आशा नहीं थी कि कोई हामी भरेगा, अत: चुपचाप उसे संग ले आई हूं. देर शाम तक लोगों का आना-जाना लगा रहा, अच्छा हुआ पड़ोसवाली आंटी पिछले दरवाज़े से चाय लाकर पिला गईं. खाना लाने की भी ज़िद कर रही थीं. बड़ों का तो कुछ खाने का मन ही नहीं और दीदी की दोनो बेटियां अपने घर पर हैं. मुन्ने के लिए आंटी खाना ले आई हैं और उसे खिला दिया है. पापा को भी उनके कमरे में लिटा दिया है. जगे हैं या सोए पता नहीं. आज की रात मैं एकदम अकेली बैठना चाह रही थी मां के पास. आज मुझे उनसे बहुत-सी बातें करनी हैं."
पिछले चार वर्षों से मन में दबी सब बातें. जो पहले चाहकर भी नहीं कह पाई. बहुत से प्रश्न हैं मन में. अपना हर दर्द बांटना है मां के साथ, आज ही. फिर कभी नहीं आएगा यह अवसर. यूं तो मां बिन कहे ही हमारा दर्द समझ लिया करती थीं, परंतु मेरा मन तो तब तक हल्का नहीं होगा न, जब तक मैं सब कुछ मां से कह न दूंगी. सो मैंने बेटे को दीदी के पास लिटा उनसे कहा कि अभी वे सो लें. मुझे जब नींद आएगी उन्हें जगा दूंगी. पंडितजी कह रहे थे कि गरुड़ पुराण के अनुसार, जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता, आत्मा मृत देह के ऊपर मंडराती रहती है. उपस्थित जन के मन की बात भी सुन-समझ सकती है, तो मेरे मन की बातें मां तक क्यों नहीं पहुंचेंगी? याद नहीं पिछली बार मां के पास इत्मिनान से कुछ देर कब बैठी थी? भागती-दौड़ती आती रविवार को, वह भी कुछ ही समय के लिए. महीने में एक रविवार अस्पताल में इमर्जेंसी ड्यूटी लगती, सो उस बार आना न हो पाता. और कभी घर में ही काम का ढेर इकट्ठा हो जाता, तब भी न आ पाती. अरसा हो गया मां के पास बैठ, उनसे बातें किए हुए. “तुम कहती थी मां कि बेटियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगी, तो उन्हें पराश्रित का जीवन नहीं जीना पड़ेगा. अपनी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत के लिए पति के आगे हाथ नहीं पसारने होंगे. आत्मनिर्भर तो हो गईं वे, पर अब तो उन्हें दो मोर्चों पर एक संग जूझना पड़ रहा है मां. पहले जब वह स़िर्फ घर और बच्चे संभालती थी, तब की बात और थी, परंतु अब भी भले ही वह पति की तरह पूरा दिन नौकरी करके, थककर घर लौटे, घर और बच्चे संभालना आज भी पत्नी का ही दायित्व है. मुश्किल यह है कि हमने अपनी बेटियों को तो मज़बूत बना दिया, पर अपने बेटों की सोच नहीं बदली. बेटियों को बेटों के बराबर पढ़ा रहे हैं, उनके मन में सपनों के बीज बो रहे हैं, उन्हें पूरा करने के अवसर दे रहे हैं, किन्तु बेटे आज भी घर के राजकुमार हैं, जिनकी ज़रूरत का ख़्याल रखना घर की स्त्रियों का कर्त्तव्य है. आज भी उन्हें परोसी थाली चाहिए सामने. बच्चे की चिंता से मुक्त जीवन चाहिए उन्हें. लेकिन पत्नी जब दिनभर की थकी घर आती है, तो उसकी देखभाल करने के लिए कौन बैठा होता है उसके इंतज़ार में? दोनो मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है उसे. आर्थिक स्वतंत्रता तो पा ली, परंतु न ही दिन के घंटों में बढ़ोतरी हुई, न ही विधाता ने उसके चार हाथ कर दिए. देखा जाए, तो पुरुष भी उसी घर का हिस्सा है, उसी घर में रहता है. खाता-पीता है, तो उस घर के कामों में पत्नी का साथ देना उसका काम क्यों नहीं? यह पत्नी पर एहसान क्यों? जब धन अर्जन में पत्नी बराबर का सहयोग दे रही है, तो घर संभालने में वह क्यों साथ नहीं दे सकता?
दरअसल हमारे पुरुषप्रधान समाज ने घर के काम को कमतर दर्जा दिया, क्योंकि वह सीधे आय से नहीं जुड़ता था और इसलिए उसे करना वह अपनी हेठी समझने लगा. काम की अधिकता, नौकरी का तनाव, यह कैसा जीवन हो गया है मां जहां अपनी ही सुध लेने की फुर्सत नहीं... मां से बात करते हुए मुझे अनेक बार बीच में झपकी आई. दिनभर के काम की थकावट थी, पर मैं अर्द्ध निद्रा में भी मां से सवाल-जवाब करती रही.
सुबह चार बजे जब दीदी की नींद खुली और वह उठकर आईं, तो मैं वहीं ज़मीन पर ही लेटी थी मां की तरफ़ मुंह किए. दीये की लौ मद्धिम पड़ चुकी थी, सो पहले तो दीदी ने उसमें घी डाला. तब तक मैं भी अच्छे से जाग गई. अब मेरा चित्त पूरी तरह शांत था. मां से अपनी बात कह मन हल्का हो चुका था. मां ने जाने कैसे, शायद स्वप्नावस्था में ही मुझे बहुत कुछ समझा दिया था. ‘हम सबसे मिलकर ही तो बना है यह समाज, तो इसमें सुधार लाना भी हमारा ही कर्त्तव्य है, हम सब का. विशेषकर हम मांओं के हाथ में है इसे बदलना, हमारे-तुम्हारे हाथ में. अपने बेटे को तुम्हीं समझाओगी यह नई सामाजिक व्यवस्था, घर के कामों का महत्व, पुरुषों के योगदान की ज़रूरत... सब कुछ. समाज को बदलने में समय लगता है मेरी बिटिया, पर वह बदलता ज़रूर है विश्वास रखो.’

अधिक कहानियां/शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए यहां क्लिक करें – SHORT STORIES