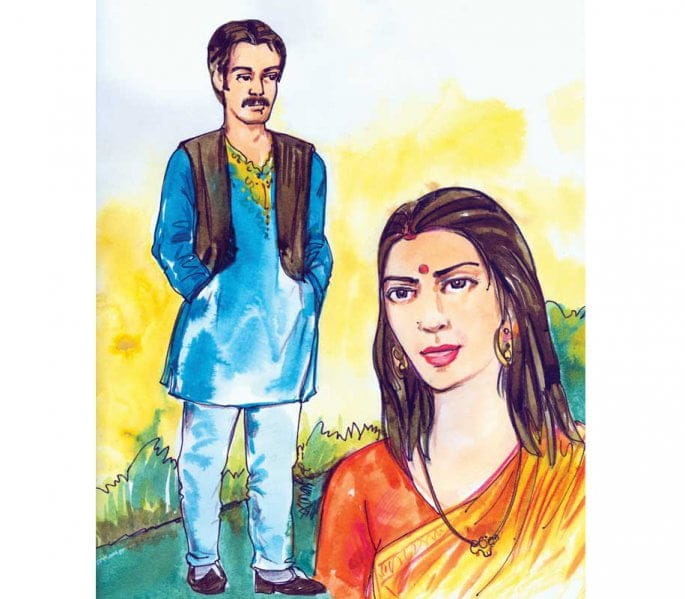काफ़ी अरसा बीत गया. जो बातें मैं तब न समझती, वह अब समझने लगी थी, महसूस करने लगी थी. मामीजी की अकेली रातों की वीरानगी और उससे भी बढ़कर उनके भीतर छिपा पराजय का बोध... परित्यक्ता का अपमान... किससे बांटती होंगी वे अपने मन का दर्द?
आज मामीजी की अंत्येष्टि भी हो गई. यह जो भीड़ उमड़ी है, मामीजी के लिए कम, मामाजी के रसूख़ के कारण अधिक है. लग रहा है मानो आधा शहर ही आ पहुंचा है यहां.
हमारे नानाजी आज भी गांव के पैतृक मकान में ही रहते हैं. उनकी वहां बहुत इ़ज़्ज़त है. बेटे के पद के कारण नहीं, अपनी विद्वता, सत्यनिष्ठा एवं सब की सहायतार्थ हाथ बढ़ाने की तत्परता के कारण. उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित नानाजी के एक मित्र अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे अर्थात् हमारे मामाजी के लिए लेकर आए, इस विश्वास के साथ कि पिता के संस्कार बेटे ने भी पाए होंगे. नानाजी ने फौरन हामी भर दी. पर जो गुण नाना-नानी में रचे-बसे थे, उन्हीं गुणों का खोखला आवरण ओढ़े बेटा राजनीति में कूद गया था, जहां इन गुणों का ढकोसला तो किया जाता है, लेकिन सचमुच उन्हें अपने जीवन में उतारा नहीं जाता. वास्तविक आचरण तो इसके ठीक विपरीत भी बना रह सकता है. मंत्री नहीं बन पाए तो क्या, प्रांत के विधायक तो हैं ही हमारे मामाजी. अनेक लोग ऋणी हैं उनके. किसी का तबादला रुकवाना हो या करवाना हो, सब कुछ करवाने में सक्षम हैं वे.
और मामीजी...? उनकी क्या हैसियत थी? शोक-सभा में आए लोगों की बातें सुन अंदाज़ा लगा सकते हैं, “गरीब परिवार की बेटी इतने ऊंचे पदाधिकारी की बीवी बनी बैठी थी, और क्या चाहिए था उसे? रानी बनाकर रखा था झा साहब ने. ऐश कर रही थी, इतने बड़े राजपाट से उठकर चली गई बेचारी.”
कहनेवालों में अपरिचित लोग तो थे ही, साथ ही उनके निजी मित्र और रिश्तेदार भी थे. मेरा जी चाह रहा था उनका मुंह बंद कर दूं किसी तरह और चीख कर कहूं, ‘सच नहीं जानते हो तो चुप तो रह ही सकते हो. मुझसे पूछो, मैं जानती हूं सच. यदि मृत व्यक्ति अपने लिए इंसाफ़ नहीं मांग सकता, तो हम जीवित होकर भी मुंह सिए बैठे रहें क्या?’ पर इन सबका क्या क़सूर? जब मैं चाहकर भी और सब जानते हुए भी सच बोलने का साहस नहीं कर पा रही थी.
नानाजी की परख एकदम सही निकली थी. अपनी कर्मठता से मामीजी ने पूरे घर को तो संभाला ही, साथ ही अपने स्नेहिल व्यवहार से सबका मन भी जीत लिया. घर की परंपराओं, संस्कारों को यूं अपना लिया जैसे इसी घर में पली-बढ़ी हों.
हमारे रिश्तेदारों में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो, जिसके किसी न किसी सदस्य ने शहर जाकर मामीजी का आतिथ्य न पाया हो. कोई इलाज के लिए जाता, तो किसी को विदेश जाने के लिए वीज़ा बनवाना होता, कोई शादी की ख़रीददारी करने जाता, तो कोई अपनी बेटी के लिए वर देखने. बिना झिझक के चले जाते सब. मामाजी को तो अपने रिश्तेदारों के नाम तक याद नहीं रहते. पर मामीजी के भीतर स्नेह की अविरल धारा ही बहती थी, जो अपने-पराये सभी को समान रूप से तृप्त करती थी. सबका मन जीत रखा था मामीजी ने. नहीं जीत पाईं तो बस अपने पति का मन.
विज्ञान के विषय लेकर मैंने बारहवीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी. डॉक्टर बनने की धुन सवार थी मुझ पर, जिसके लिए कोचिंग की ज़रूरत थी. मम्मी ने मुझे अपने छोटे भाई के घर शहर भेज दिया. हां, यही तो कहते थे सब कि मैं अपने मामाजी के घर रहती हूं. ठीक ही तो है, घर तो सदैव पुरुष का ही होता है न! चाहे उसमें स्त्री अपना सर्वस्व ही समर्पित क्यों न कर दे. तिस पर एक अति कठोर मास्टर के रूप में हमारे मामाजी थे. ज़रा-सी चूक हुई नहीं कि लगते डांटने-डपटने.
उनकी कोई संतान नहीं थी. मामीजी ने अपने सब परीक्षण करवा लिए थे. उनमें कोई दोष नहीं था. डॉक्टरों के अनुसार मामाजी को अपने परीक्षण करवाने चाहिए थे. पर यह कैसे हो सकता था? पुरुष में भी कभी कोई दोष हुआ है क्या? और मामाजी बिल्कुल राज़ी नहीं हुए डॉक्टर के पास जाने के लिए. पर बांझ होने की गाली मामीजी ताउम्र सुनती आईं.
शहर आकर मामीजी अपना देहाती परिवेश छोड़ पूरी तरह से आधुनिका बन गई थीं. पढ़ी-लिखी तो थीं ही, पहनावा भी शहरी अपना लिया था. मामाजी की उन्नति के साथ-साथ अपना रहन-सहन, बोलचाल का ढंग- सब बदल लिया था, ताकि मामाजी को कभी किसी के सामने शर्मिंदा न होना पड़े. पर मामाजी को तो अपनी पत्नी में मीनमेख निकालने का सामाजिक अधिकार ही मिला हुआ था. वे हमेशा कोई न कोई नुक्स निकालते रहते.
मामाजी के पास सहायतार्थ लोग आते ही रहते थे. ऐसे ही कभी गायत्री भी आई थी. तब मैं वहीं रहती थी. मैंने भी देखा था उसे. नव खिली कली-सी, विधाता ने असमय ही उसके माथे का सिंदूर पोंछ दिया था और द़फ़्तर के बाबू आधिकारिक रूप से उसे मिलनेवाली पेंशन दबाकर बैठे थे. अतः फ़रियाद लेकर गायत्री आई थी मामाजी के पास. मामाजी ने तो कभी आत्मीय जनों का काम भी न किया होगा बदले में कुछ पाने की उम्मीद लिए बिना, तो उसका कैसे करते? और रिश्वत केवल पैसों की ही शक्ल में ली जाती है क्या?
हमारी नैतिक मर्यादाएं, सामाजिक नियम-क़ानून ये सब स्त्रियों के लिए ही बने हैं. मामाजी को गायत्री भा गई. संभव है, गायत्री ने पहली बार समर्पण अनिच्छा से ही किया हो. पर उसके न कोई आगे था, न पीछे. शहर के इतने शक्ति संपन्न व्यक्ति का संरक्षण मिल रहा था उसे और यूं स्थाई ही हो गया उनका संबंध.
पत्नी की भावनाओं का विचार करके नहीं, अपितु अपनी प्रतिष्ठा की ख़ातिर गायत्री को शहरी सीमा के बाहर घर ले दिया था मामाजी ने. दिनभर मामाजी अपने सरकारी आवास पर रहते. लोगों से मिलना-मिलाना, सरकारी काम सब वहीं से निबटाते. पर अंधकार की चादर बिछते ही वह अपनी प्रिया के पास पहुंच जाते और क्षेत्र का दौरा करने के बहाने दो-एक दिन के लिए ग़ायब रहते, पर उनका पड़ाव वहीं होता था.
बहुत क़रीबी रिश्तेदार या चंद मित्रों को छोड़ बाकी सबके लिए वे साफ़-पाक, आदर्श पति ही बने रहे सदैव.मुझे मेडिकल कॉलेज में दाख़िला लिए सालभर हुआ होगा, जब मामाजी और गायत्री के संबंध की चर्चा मैंने पहली बार सुनी. मम्मी ने मेरे सामने इस बारे में कोई बात कभी नहीं की. ये सब तो मैंने नानी से उनके संग हुई बातों से जाना. मैं देख रही थी कि मम्मी, नानी समेत सब संबंधियों ने मामीजी से दूरी बना ली थी. अब मम्मी मामीजी से पहले की तरह फ़ोन पर घंटों बातें न करतीं. नानी भी तीज-त्योहार की याद न दिलाती. मेरे मन को बहुत ठेस लगी. मैं आज जिस मुक़ाम पर पहुंची थी, उसका पूरा श्रेय मामीजी को ही जाता था. उन्होंने स़िर्फ कर्त्तव्य पूरा करने जैसी देखभाल नहीं की थी मेरी. बेटी जैसा स्नेह भी दिया था मुझे. मैं मम्मी और नानी को समझाने का प्रयत्न करती, पर बड़ों के सामने बढ़-चढ़कर बोलने का अधिकार बच्चों को नहीं था. बेटियों को तो बिल्कुल नहीं और मेरे सब संबंधियों ने भी मामीजी से दूरी बना ली थी.
काफ़ी अरसा बीत गया. जो बातें मैं तब न समझती, वह अब समझने लगी थी, महसूस करने लगी थी. मामीजी की अकेली रातों की वीरानगी और उससे भी बढ़कर उनके भीतर छिपा पराजय का बोध... परित्यक्ता का अपमान... किससे बांटती होंगी वे अपने मन का दर्द? कितना भी प्रयत्न करतीं, लेकिन उम्र में अपने से 15 वर्षीया कम युवती का मुक़ाबला वो कैसे कर पातीं? उम्र तो अपने पंजों के निशान स्त्री-पुरुष दोनों पर समान रूप से छोड़ती है न. पर स्त्री तो पति की दीर्घायु की कामना करती रहती है तमाम जीवन. फिर पुरुष ही क्यों अपनी ब्याहता को भूल, नई खिली कली को देख उधर ही दौड़ पड़ता है?
पर कुछ प्रश्न पूछे नहीं जाते शायद... सवाल तो और भी हैं, अधिक पेचीदा, अधिक उलझे हुए, जिनके उत्तर आज तक तलाश रही हूं मैं. उलझे धागों की तरह कभी कोई सिरा मिलता भी है तो अगले पल फिर गुम हो जाता है. उलझ गए धागों को सुलझाना आसान काम है क्या? क्यों किया मेरे संबंधियों ने मामीजी के साथ ऐसा बर्ताव? किसी ने हमें कष्ट पहुंचाया हो, हम पर अत्याचार किया हो, तो उसके प्रति हमारे मन में क्रोध उपजे और उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश की जाए, यह बात तो कोई भी समझ सकता है, किंतु अजब इंसानी फ़ितरत है कि जिसके प्रति हमने स्वयं अथवा हमारे किसी आत्मीय ने अन्याय किया हो, उससे ही हम कन्नी काटने लगते हैं, बजाय उससे हमदर्दी जताने के. यही कर रहे थे मेरे अपने भी. हिम्मत नहीं थी उनमें मामीजी की नज़रों का सामना करने की. अतः उन्होंने मामीजी से दूरी बना ली. सब जानते थे कि मामाजी क़सूरवार हैं. मामाजी के विमुख होते ही सब रिश्ते बेमानी हो गए. अपने टूटे सपनों की किरचों पर अकेली ही बैठी रह गईं मामीजी. वे सब, जिन्हें उन्होंने अपना ही परिवार माना था, अनदेखा कर मुंह फेरे खड़े रहे.
विवाह के समय लड़की पति का नाम धारण कर अपनी पुरानी अस्मिता तक पूरी तरह मिटा डालती है. पर इतना काफ़ी नहीं है शायद? मामीजी का ब्लडप्रेशर हाई रहने लगा था, जिसके लिए नियमित रूप से दवा लेते रहना ज़रूरी था. पर लगता है वह ठीक से दवा ले नहीं रही थीं. क्या वह अपने जीवन से निराश, जान-बूझकर ही ऐसा कर रही थीं? कौन बताएगा? यदि ठीक से दवा ली होती, तो शायद स्ट्रोक न होता, ऐसा कहना था डॉक्टरों का. स्ट्रोक हुआ भी तो आधी रात को. पास तो कोई था नहीं, अतः बेहोशी की हालत में सुबह तक पड़ी रहीं. सुबह अस्पताल तो ले जाई गईं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी. यदि ठीक समय पर ले जाई गई होतीं, तो बच सकती थीं .
मामीजी को गुज़रे छह माह बीत चुके थे. उस मौ़के पर हम सब गए थे, तो उसके बाद हम चाहकर भी दुबारा नहीं जा पाए थे. फिर कभी मम्मी को काम आन पड़ता और कभी मामाजी व्यस्त होते. इस बार मम्मी ने जाने का दृढ़ निश्चय किया तो मेरा भी मन हो आया साथ जाने का. मैं अब डॉक्टर बन चुकी थी और एम.डी. में मेरा दाख़िला भी हो चुका था. मामीजी मेरी आदर्श थीं. उनके न रहने पर भी एक बार फिर मैं उस घर में मामीजी की उपस्थिति महसूस करना चाहती थी. उनके एहसास को अपने चारों ओर जी लेना चाहती थी, ज़ज़्ब कर लेना चाहती थी अपने भीतर सदा के लिए.
मैंने मामाजी के घर फ़ोन मिलाया तो इस बार उनके पी.ए. की जगह एक महिला की आवाज़ सुनाई दी. कहीं ग़लत नंबर न लगा हो, यह सोच मैंने मामाजी का नाम लेकर उनसे बात करवाने को कहा. उधर से उत्तर मिला कि अभी वे व्यस्त हैं और मैं एक घंटे के बाद फ़ोन करूं. उनके इतने फ़ोन आते रहते होंगे कि उस स्त्री ने मेरा परिचय जानना भी ज़रूरी नहीं समझा. पर फ़ोन रखने से पहले मैंने ही उत्सुकतावश पूछ लिया, “आप कौन बोल रही हैं?”
दूसरी ओर से उत्तर मिला, “गायत्री, उनकी धर्मपत्नी...”
मैं जानती हूं कि मैं उन्हें ‘मामी’ कभी नहीं कह पाऊंगी. पर इससे फ़र्क़ ही किसे पड़ता है? जब कुछ कहना चाहिए था, करना चाहिए था तब कुछ नहीं किया. साहस नहीं जुटा पाई या ये कहें कि तब मैं इतनी परिपक्व नहीं थी कि स्थिति की गंभीरता को समझ पाती. पर आज मेरी आप सभी से यही गुज़ारिश है कि ऐसी स्थिति में अपने-पराये का भेद त्याग उस व्यक्ति का साथ दें, जिसके साथ अन्याय हो रहा हो. ज़िंदगी जब उठा-पटक करती है तो शरीर नहीं, मन लहूलुहान होता है और ऐसे में अपनों का साथ ज़ख़्मों पर मरहम का काम करता है.