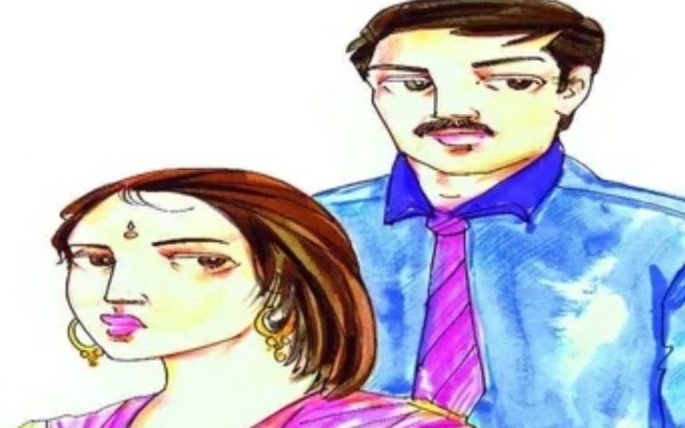शहर में देवदास फ़िल्म लगी, तो मित्र-मंडली चल पड़ी देखने. फ़िल्म अच्छी थी या बुरी- इस झंझट में कौन पड़े. बस सबको एक नाम मिल गया था ‘देवदास’. कोई लड़का ज़रा ग़मग़ीन दिखा, तो झट उसे फिकरा सुनने को मिलता ‘क्या देवदास बने बैठे हो.’ कोई लड़का किसी लड़की की तरफ़ ज़रा झुका नहीं कि उसे देवदास का ख़िताब मिल जाता. मेरा मन भी बांवरा होने लगा था अपनी पारो के लिए.
शरद की डायरी से- साठ पार कर चुका हूं. दो-दो बार नाना और दादा बन चुका हूं, पर आज भी जब आंखें मूंद लेटता हूं, तो वह मुस्कुराती हुई सामने आ खड़ी होती है. वही बीस वर्षीया, खिलती कली सरीखी. और मैं यह भूल जाता हूं कि मैं पचास-साठ तेज़ी से पार करता जा रहा हूं. मन किसी युवक के मन-सा धड़कने लगता है और चेहरे पर ख़ुशी की लहर दौड़ जाती है. ज़रा-सा भी परेशान होने पर वह खिलखिलाती हुई पास आ बैठती है और कहती है, “क्यों उदास हो शरद? ऐसे उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते है. सब ठीक हो जाएगा.” मन फिर उत्साहित हो उठता है. मैं वैसे ही आंखें मूंदे पड़े रहना चाहता हूं, उसके क़रीब होने का एहसास लिए. जानता हूं कि आंख खोलूंगा, तो वह कहीं नहीं होगी. आसपास तो क्या, दूर-दूर तक कहीं नहीं होगी. ऐसा नहीं कि मैं सत्य का सामना नहीं करना चाहता था, पर डरता हूं मैं यथार्थ से. नहीं! कुछ भी कमी नहीं है मेरे जीवन में. एक नेक और समझदार जीवन संगिनी, अच्छे स्नेहिल बच्चे और होनहार नाती-पोते. किसी बात का गिला नहीं मुझे विधाता से. कोई यह भी नहीं कह सकता कि मैंने अपने कर्त्तव्यों की पूर्ति में कोई कमी रखी. आदर्श पति और आदर्श पिता के सारे फ़र्ज़ पूरी तरह से निभाये हैं मैंने. केतकी को खोने के बाद शायद पत्नी को अतिरिक्त सहेज-संभालकर ही रखा है? उसके हर सुख-दुख में साथ दिया है. केतकी का ख़याल तो एक मधुर-सा एहसास बनकर आता है और माहौल को महका जाता है. हमारे पड़ोस में ही रहती थी वह. दो बहनों में बड़ी, चपल और बातूनी. पड़ोसी होने के नाते प्रायः ही आना-जाना, मिलना-मिलाना लगा रहता उस कस्बई शहर में. उनके कोई बेटा नहीं था, सो देर-सवेर, व़क़्त-बेव़क़्त ज़रूरत पड़ने पर मुझे गुहार लग जाती. मेरी कोई बहन नहीं थी, तो मां को जब भी कोई बड़ा आयोजन करना होता, तो केतकी को बुला लेती. केतकी के पिता को जब दिल का दौरा पड़ा, तो अस्पताल की सारी भाग-दौड़, रात को उनके पास रुकने की ज़िम्मेदारी सब मैंने संभाल ली. दुख-दर्द प्रायः ही लोगों को क़रीब ला देता है. एक अपनेपन का एहसास तो पहले से ही था, इस बीमारी के दौरान हम एक-दूसरे के और भी क़रीब आ गये. कॉलेज के दिन भी क्या मस्तीभरे दिन होते हैं. न घर-गृहस्थी की फ़िक्र, न पैसा कमाने की चिंता. शहर में देवदास फ़िल्म लगी तो मित्र-मंडली चल पड़ी देखने. फ़िल्म अच्छी थी या बुरी- इस झंझट में कौन पड़े. बस सबको एक नाम मिल गया था ‘देवदास’. कोई लड़का ज़रा ग़मग़ीन दिखा, तो झट उसे फिकरा सुनने को मिलता ‘क्या देवदास बने बैठे हो.’ कोई लड़का किसी लड़की की तरफ़ ज़रा झुका नहीं कि उसे देवदास का ख़िताब मिल जाता. मेरा मन भी बांवरा होने लगा था अपनी पारो के लिए. उसकी मनमोहक मुस्कुराहट, खनकती-सी खिलखिलाहट सोते-जागते मेरे सम्मुख रहने लगी थी. यह भावना इतने धीरे और चुपके से मन में समाई थी कि मुझे स्वयं ही इसका पता नहीं चला था. पर लगता है, मुझसे पूर्व मेरी मां ने ही मेरे इस झुकाव को ताड़ लिया था और वह मेरी पसंद से ख़ुश भी थी. तभी तो वह केतकी को बहाने से बुला लेतीं. उसे घर के रीति-रिवाज़, भोजन में हमारी पसंद-नापसंद से अवगत कराती रहतीं. पर तभी हमारे प्यार पर कहर टूट पड़ी. केतकी से मेरे विवाह की बात करते ही पिताजी भड़क उठे. मां ने मनाने की बड़ी कोशिश की, पर वे नहीं माने. तब समझ में आयी थी मुझे देवदास की तड़प. उसकी टूटकर बिखर जाने की प्रचंड उत्कण्ठा. कसूरवार था मैं अपनी केतकी का, पर बहुत मजबूर भी था. इतनी हिम्मत न थी, न ही ऐसे संस्कार थे कि पिता से विद्रोह करके केतकी से विवाह कर लेता. मैं बेबस देखता रहा और वह किसी और के साथ ब्याह दी गई. ऐसा नहीं कि मन में पीड़ा की कमी थी, पर मुझे उसे अपने अंतस में दबाकर रखना था. कठिन परीक्षा की घड़ी थी मेरे लिए. तीन-चार माह लग गये मुझे संभलने में, अपनी स्थिति से समझौता करने में. पर एक बात पर मैं दृढ़ था. मैं देवदास की भांति निराशा के गर्त में नहीं डूबूंगा. एक क़िस्म से आत्महत्या ही तो थी, जो देवदास ने किया था शराब में ख़ुद को डुबोकर. यथार्थ का सामना करने का साहस नहीं था उसमें. क्या यूं परिस्थितियों से घबराकर, टूटकर बिखर जाना सही है? केतकी की छोटी बहन के विवाह के समय अंतिम बार देखा था उसे. बातचीत भी हुई थी. तब सोचा था, मैत्री तो बनाए ही रख सकते हैं. पर नहीं... मैत्री तभी तक सीमा में रह सकती है जब एक-दूसरे के प्रति कभी आकर्षण रहा हो. मिलने पर कभी पुरानी टीस जाग उठी तो? अब वह किसी के घर की मर्यादा है. मैं किसी भी क़ीमत पर उसकी ख़ुशी में विघ्न नहीं बन सकता. उचित यही था कि हम कभी न मिल पाएं. वह प्यार और सम्मान जो मैं उसे न दे सकता, वो सब उसे वहां मिले, यही दुआ थी मेरी. कथा केतकी की- जैसे-जैसे मेरा बेटा विदुर यौवन की दहलीज़ पर क़दम रखने लगा, प्रायः ही मुझे शरद की याद दिला जाता. वही सौम्य-शालीन व्यवहार, वही धैर्य, दूसरों के दुख-तकलीफ़ में वही भागीदारी. कहां से आए उसमें ये सब गुण? ख़ून के रिश्तों में तो वंशानुगत गुणों की व्याख्या हो चुकी है- पर मन से कोई जुड़ा हो- बहुत गहरे तक, किसी को बहुत शिद्दत से याद किया हो, तो क्या उसके गुण भी आ सकते हैं गर्भस्थ शिशु में? इस विषय पर भी क्या कोई मनोवैज्ञानिक शोध करेगा? अजीब बात है ना. न उसने कभी स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह मुझे कितना चाहता है, न मैंने ही ये सब सुनने की उम्मीद रखी. एक अनकही-सी समझ थी हम दोनों के बीच. और कुछ कहने-सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. तब आज की तरह आज़ादी नहीं थी, विशेषकर लड़कियों के लिए. बाल कटवाना फैशन की सीमा थी और कोई लड़की स्लीवलेस कपड़े पहनने लगे अथवा पारंपारिक वेशभूषा छोड़ पैंट पहनने लगे, तो चर्चा का विषय बन जाए. ख़ासकर छोटे शहरों में तो स्थिति ऐसी ही थी. फ़िल्में देखीं भी तो झांसी की रानी, जागृति क़िस्म की, वह भी किसी बड़े के संरक्षण में. पर शरत् साहित्य कोर्स में होने के कारण देवदास देखने की अनुमति मिल गई, तो हम लड़कियों का पूरा ग्रुप ही चल पड़ा देखने. और मेरी सखी-सहेलियों को मुझे छेड़ने के लिए नया बाण मिल गया. शरद तब से ‘तुम्हारा देवदास’ बन गया. कितना संस्कारी, कितना संयमी था वह. मैं ही फालतू की बातें करती रहती. पर शरद की मां को तो मेरा बतियाना अच्छा ही लगता था. घर में मेहमान आने पर, पूजा-पाठ होने पर मुझे सहायता हेतु बुला लेतीं. शरद मुझे छेड़ने के बहाने कहता, “मां, तुम परेशान नहीं हो जातीं इसकी हर समय की बकबक से?” “ना रे. इसके आने से तो घर में रौनक आ जाती है. मैं तो यह बकबक स्थाई रूप से सुनने को तैयार हूं.” कह कर वह कनखियों से बेटे की तरफ़ देख मुस्कुरा देतीं. पचीस वर्ष तो हो गये होंगे उसे देखे, शायद कुछ और अधिक. पर कभी नहीं लगा कि वह मुझसे दूर है. अपनी हर छोटी-बड़ी ख़ुशी मैंने उससे बांटी है. अपनी हर परेशानी उससे कही है. जब भी अकेली बैठ कुछ काम कर रही होती हूं, तो हाथ तो उलझे होते हैं काम में, पर मन उसी से बातें करता रहता है, छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी ख़ुशियां और उलझनें- विदुर की शरारतें, कोई विशेष बनाया पकवान, कल पैर में लग गई चोट- सब कुछ. नहीं जानती उसे सामने देख एकदम से पहचान पाऊंगी कि नहीं, पर मेरी यह एकतरफ़ा बातचीत उस तक नहीं पहुंचती, इतना अवश्य जानती हूं. फिर भी मुझे अपने मन का हाल उससे बांट कर तृप्ति का एहसास होता है. ठीक किसी आत्मीय से बातचीत कर लेने के समान. नैतिकता के तराजू पर तोलोगे तो अवश्य मुझे दोषी पाओगे. मेरा उसे यूं ख़यालों में रखना ग़लत है, कहोगे. पर जो मेरे साथ हुआ, वह ग़लत नहीं था क्या? हमारी पीढ़ी आंख मूंद सब कुछ स्वीकार कर लेती थी, सो मैंने भी किया. जानती हूं, शरद किसी और का है, किसी के सिर का ताज है वह. तो रहे ना! मेरे तो मन के एकदम भीतरी कोने में बैठा है और मौक़ा मिलने पर उससे थोड़ी बातें कर लेती हूं, इतना ही तो, बस. विदुर अब बड़ा हो गया है. पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा और अब रसायनशास्त्र में शोधकार्य कर रहा है. मैंने उसे यही सिखाया है कि ज़िंदगी वह अपनी इच्छा से जी सकता है, बशर्ते उसका रास्ता सही हो, सही तरी़के से चुना गया हो. और आज मेरी परीक्षा की घड़ी है. वह अपने आधीन शोध करती एक लड़की से विवाह करना चाहता है. नहीं, आज के युग में यह कोई धमाकेदार ख़बर नहीं. बस इतना और है कि तूलिका न केवल तलाक़शुदा है, उसके साथ तीन वर्षीया बेटी भी है. विदुर को न केवल मेरी अनुमति चाहिए, उसके पिता को मनाना भी मेरे ज़िम्मे है, जो नामुमकिन तो नहीं, पर कठिन अवश्य है. अब पिता भी पहले जैसे तानाशाह नहीं रहे. मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे देवदास बने बेटे को न तो दुनिया से विमुख हो शराब में स्वयं को डुबोना पड़ेगा, न ही मन मार सारी उम्र केवल कर्त्तव्यों का पालन करते ही जीना होगा. वह घर लाएगा अपनी पारो को- मय सूद के.उषा वधवा
अधिक शॉर्ट स्टोरीज के लिए यहाँ क्लिक करें – SHORT STORIES
Link Copied