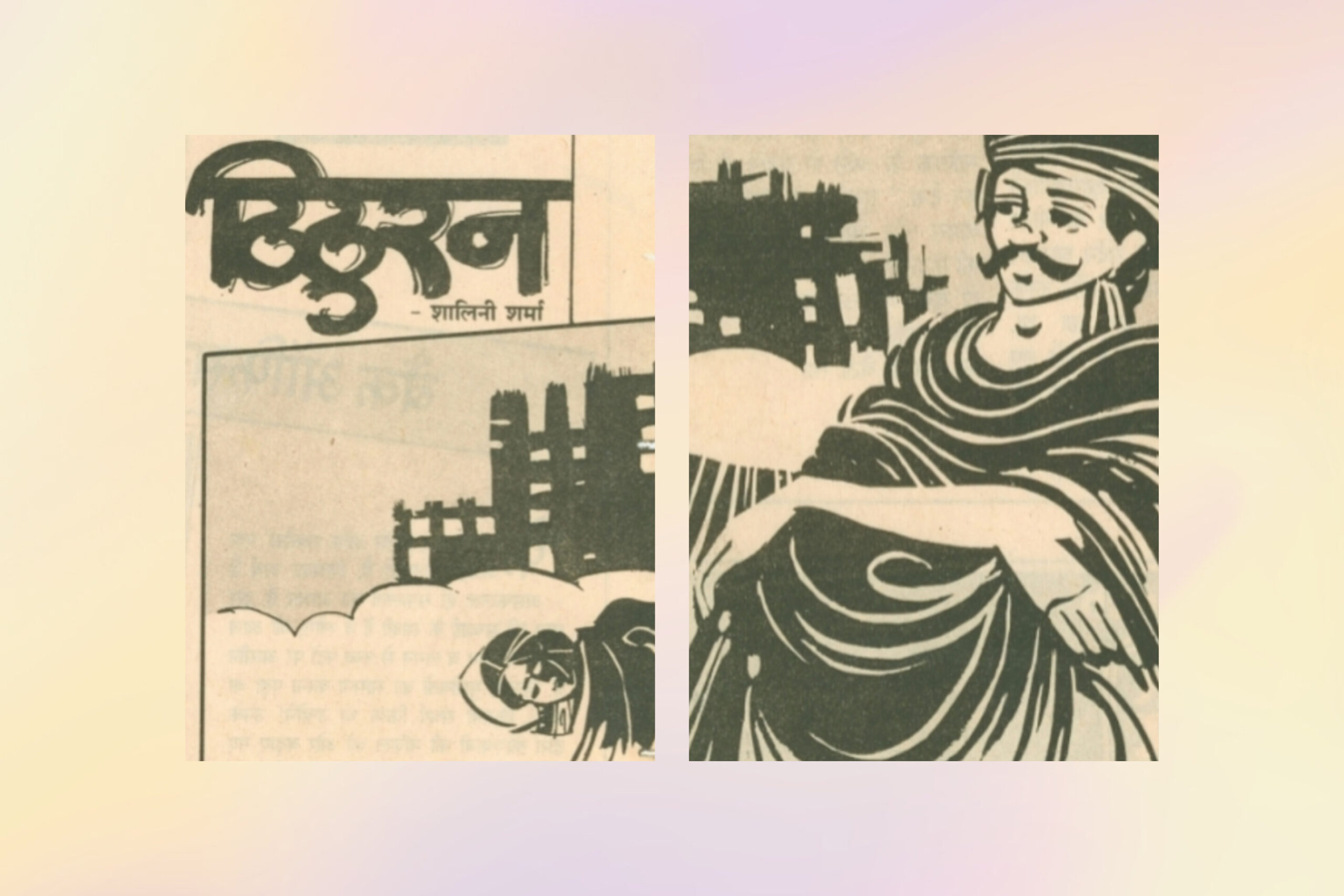वह पत्नी को डपट रहा था, "चुप करा इसे भागवान! सब लोगों की नींद ख़राब करेगा." "क्या करूं, ठंड के मारे सो नहीं रहा है. कंबल तो जैसे पानी हो गया है." पत्नी गिडगिड़ाती सी बोली. वह चुप हो गया. कुछ नहीं बोला आगे. सुखबीर कुछ क्षण न जाने क्या सोचता रहा, फिर झटके से उठा.
दिल्ली से बस जब चली थी तो सूरज निकल आया था. जाड़ों की सुबह में उगने वाले सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी थीं. किरणों में गर्मी की ताब अधिक नहीं थी. बाहर धूप धीरे-धीरे अपने पंजे फैला रही थी. खेतों में दूर-दूर तक फसल खड़ी थी. बस की खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता और पूरे बदन में एक सिहरन सी पैदा कर जाता. वह बस में कुनमुनाया सा बैठा था. बगल में पत्नी बैठी थी ख़ामोश, निस्तब्ध, उसको गोद में तीन वर्ष का बीमार लड़का था. वह खिड़की से बाहर दूर-दूर तक फैले मैदानों के परे न जाने क्या देख रही थी? उसके चेहरे पर दुख, क्षोभ और चिंता के गहरे बादल छाए हुए थे. बस घरघराती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी.
बस में बैठे दूसरे स्त्री-पुरुषों व बच्चों के चेहरों पर ख़ुशियां फैली हुई थीं. हर आधे घंटे के बाद बस में बैठा कोई न कोई यात्री ज़ोरों से चिल्ला उठता था, "प्रेम से बोलो जय माता की." उसकी आवाज़ के साथ-साथ बस में बैठे लगभग सभी यात्री एक साथ चिल्ला उठते थे, "जय माता की."
अक्टूबर महीने का अंतिम सप्ताह था. यात्रियों से भरी बस चाय-पानी के लिए जगह-जगह रुकती और फिर अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ जाती. श्रद्धालु यात्रीगण रास्ते भर गाते-बजाते, बीच-बीच में रुककर माता की जय-जयकार बोलते जा रहे थे. दोपहर बाद बस पहाड़ के घुमावदार रास्तों पर चढ़ने लगी.
वह राजस्थान के किसी दूरदराज कस्बे से आया था. दिल्ली में स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय भीड़-भाड़ में किसी ने उसकी जेब काट ली थी. पूरे डेढ़ सौ रुपए थे. चाय पीने के बाद जब उसने जेब में हाथ डाला तो अवाक् रह गया था, जेब में कुछ भी न बचा था. वह दुखी हो गया था. पत्नी ने कुछ रुपए सहेजकर रखे थे. उसने हिसाब लगाया कि पानी के पास के रुपयों में सिर्फ़ आने-जाने का ख़र्च चल सकता था. घर वापस लौटने की उसे कोई तुक नज़र नहीं आ रही थी.
स्टेशन से मुंह अंधेरे ही वह पैदल बस स्टैण्ड के लिए चल पड़ा. वह बड़ी किफायत से ख़र्च कर रहा था. बस टिकट ख़रीदने के बाद वापस लौटने के लिए. उसने टिकट के पैसे अलग से पेंट की अन्दरूनी जेब में रख लिए. वह पहले से ही मुसीबतों का मारा हुआ था. चपरासी की सरकारी नौकरी थी उसकी बेहद मामूली वेतन से ही उसका घर ख़र्च बमुश्किल चल पाता था.
बच्चा डेढ़ वर्ष से बीमार चल रहा था. न जाने कौन सी बीमारी थी उसे? शरीर सूखता जा रहा था. उसने अपनी औकात भर डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों का ख़ूब इलाज कराया, लेकिन बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. झाड़-फूंक भी उसने कराई थी अपने कस्बे के मशहूर ओझा से. कहीं कुछ नहीं हुआ तो वह हर तरफ़ से निराश हो गया. बच्चे के इलाज की खातिर उसने पत्नी के चांदी के जेवर और घर के पीतल के भारी वज़न वाले बर्तन तक बेच डाले थे.
उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी थी कि वह बच्चे को लेकर माता के दर्शन कर आए, उसका पूरा विश्वास है कि माता की कृपा से बच्चा अवश्य ठीक हो जाएगा. माता की कृपा सबको प्राप्त होती है. उसने सोचा उसे जाना चाहिए, दोस्त की बात ने उसके मन में एक नया विश्वास पैदा कर दिया था. उसने दोस्तों से मांगकर पैसे इकट्ठे किए और यात्रा पर निकल पड़ा.
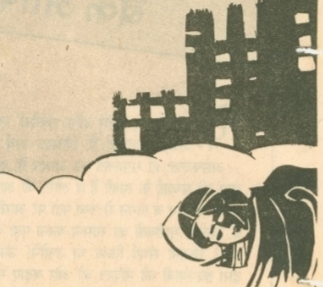
सांझ घिरने से पहले ही बस अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच गई. सामने पहाड़ी पर माता का मंदिर था. घुमावदार रास्तों वाली कठिन चढ़ाई थी. लोग सवेरे चढ़ाई शुरू करते थे और शाम तक वापस लौट पाते थे. यात्री बड़ी संख्या में ऊपर से लौट रहे थे वापस. उनके चेहरों पर पथरीली पहाड़ियों के घुमावदार रास्तों पर जाने और वापस लौटने से पैदा हुई थकान के चिह्न साफ़-साफ़ दिखलाई दे रहे थे. वह बस से उतरा और चल पड़ा.
उसने देखा, बाज़ार में भी बहुत भीड़ थी. लोग बाग दूर-दूर से आए थे. यात्रियों में हर सूबे, हर प्रान्त की औरतें, मर्द, बच्चे व कमसिन लड़कियां थीं. ख़ूब रौनक थी. बाज़ार की चहल-पहल देखते ही बनती थी. जगह-जगह पर मिठाई, खिलौने, चाट-पकौड़ी तथा प्रसाद बेचने वालों की छोटी-बड़ी दुकानें सजी थीं. सड़क के किनारों पर कुछ नेपाली युवक-युवतियां स्वेटर, शॉल, गर्म टोपे और पुलओवर बेच रहे थे. पूरे बाज़ार में एक अजीब सी ख़ुशबू ग़मक रही थी, अगरबत्तियों और धूप के जलने जैसी. धर्मशालाओं में भीड़ बहुत थी. हर जगह मेला जैसा लगा था. वह कई धर्मशालाओं में गया. जगह कहीं भी नहीं थी. एक धर्मशाला का मुनीम दरवाज़े पर खड़ा हाथ जोड़-जोड़कर आने वाले यात्रियों से जगह न होने के लिए क्षमा याचना कर रहा था.
यह भी पढ़ें: 10 बातें जो हर पिता को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए (10 Things Every Father Should Teach His Kids)
उसने देखा, एक ओर खुले मैदान में टीन की चादरों और बांस की बल्लियों से बनाए गए बड़े-बड़े झोपड़ेनुमा हॉल से थे, जिनकी छतें भी टीन की चादरों और बांस आदि से पाटी हुई थीं. यात्रीगण उधर भी जा रहे थे. वह भी उस तरफ़ चल दिया, अंधेरा घिर आया था. वह एक बड़े से झोपड़े के सामने आकर ठहर गया, दरवाज़े के अंदर की तरफ़ एक कोने में पेट्रोमैक्स जल रहा था. अंदर दो आदमी एक चौकी पर बैठे थे. उनकी बगल में दो ढेर रखे थे. एक मोटे-मोटे गद्द्दों का और दूसरा लिहाफों का. झोपड़े के बाहर एक कोने में चाय की छोटी सी दुकान थी. दुकान पर एक बूढ़ा सिर पर गोल टोपी लगाए अपनी कथरी में लिपटा बैठा था. अंगीठी पर केतली चढ़ी थी.
अंगीठी से सटकर एक छोटा-सा लड़का कुड़कुड़ाया सा बैठा था ऊकड़ू. रात गुज़ारने वाले यात्री अंदर बैठे आदमी से गद्दे और लिहाफ लेकर अंदर ज़मीन पर बिछी चटाई के ऊपर अपने बिस्तर लगा रहे थे.
ठंड बढ़ चली थी, किसी हद तक शरीर को कंपकंपा देने वाली. कभी-कभी सर्द हवा का झोंका आता और पूरे शरीर को भीतर तक हिला डालता. वह पत्नी सहित अंदर आ गया. उसने सामने बैठे अधेड़ से शख़्स से पूछा, "गद्दे का क्या लेते हैं?"
"दो रुपए गद्दा, पूरी रात के लिए." झोपड़े के मालिक गनपत ने जवाब दिया.
"और लिहाफ का क्या लेते हैं?" उसने फिर पूछा.
"उसके भी दो रुपए." गनपत ने अन्यमनस्क भाव से उत्तर दिया.
"कुछ कम नहीं हो सकता है?" उसने धीरे से पूछा.
"भाई, दो रुपए क्या ज़्यादा है? दूसरे डेरों पर तो ढाई से कम नहीं मिलेगा, हमारा रेट सही है. इससे कम न होगा." गनपत के नौकर सुखबीर ने जो वहीं बराल में बैठा था, समझाने के लहजे में कहा.
वह चुप हो गया. उसने कुछ सोचा, फिर दो रुपए का नोट निकाला और सुखबीर को पकड़ा दिया. गद्दा उठाने लगा तो पीछे से पत्नी ने कहा, "एक लिहाफ भी ले लो ना." उसने पत्नी की ओर देखा और कुछ क्षण रुककर बोला, "कम्बल है तो अपने पास."
"एक कम्बल में तीन जने कैसे सोएंगे भला, सोचो तो, ठंड़ कितनी है." पत्नी ने अनुरोध भरे स्वर में कहा.
"मेरे लिए तो लोई ही काफ़ी है." उसने कहा और बदन पर लपेटी हुई लोई को सिर पर बांध लिया, पत्नी चुप हो गई बेचारी. उसने गद्दा ले जाकर एक कोने में बिछा दिया. पत्नी ने बच्चे को गद्दे पर लिटा दिया और उसे अपने पास खींचकर कम्बल ओढ़ लिया. वह जानती थी कि पति पैसे की तंगी की वजह से खीजा हुआ है. उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी और वह इस आशंका से छिपी हुई थी कि कहीं बच्चे को ठंड लग गई तो क्या होगा? वह भी पत्नी की मनोदशा को समझ रहा था, मगर उसके पास पैसे बहुत कम थे.
परदेस का मामला था. न जाने कब-क्या हो जाए? वह स्वयं ही अजीब असमंजस में पड़ा हुआ था. जेब काटने वाले को उसने मन ही मन ढेर सारी बददुआएं दे डाली. वह लोई को कान तक लपेटे बैठा था और थोड़ी-थोड़ी देर बाद बीड़ी सुलगा लेता था. सुखबीर उसे देख रहा था. काफ़ी देर बाद झोपड़े का मालिक गनपत अपने डेरे पर चला गया,
गनपत पास ही के एक गांव का रहने वाला है. वह हर साल जाड़ों में यहां आ जाता है. वह मैदान से आने वाले यात्रियों की नब्ज़ पहचानता है. उतरते और चढ़ते जाड़ों तक, यानी छह महीने यात्रियों का रेला पेला जोर-शोर से आता है. बाक़ी के छह महीनों में तो इक्के-दुक्के यात्री ही आते हैं. धर्मशालाओं के कमरे खाली पड़े रहते हैं. उस समय कौन आता है झोपड़ियों में. वह अपने रेट सही रखता है. भीड़ देखकर दूसरों की तरह बढ़ाता नहीं है.
यह भी पढ़ें: वास्तु के अनुसार कैसा हो घर का मंदिर? (How should the home temple be according to Vastu?)
सुखबीर उसी के गांव का रहने वाला है. हर साल उसके साथ आता है. उसे खाना और दो सौ रुपए माहवार मिलता है. गनपत ने उसे कह रखा है कि न रेट बढ़ाने की ज़रूरत है और न कम करने की. चाहे कोई भी क्यों न हो, कोई छूट नहीं देनी है. उसका कहना है कि इसी आमदनी से तो साल-भर का घर ख़र्च चलता है. हम धंधा करने आते हैं, कोई धरम कमाने नहीं. ये लोग तो सालों में एक बार पुण्य कमाने आते हैं.
रात के बारह बज गए थे. टीन की चादरों की बारीक फांकों से ठंडी हवा छन कर आ रही थी. वह सिकुड़ा हुआ गठरी बना बैठा था. बीड़ी के धुंए से उसके शरीर में कोई गर्माहट नहीं पहुंच रही थी. ठंड उस पर सीधे-सीधे वार कर रही थी. उसने बैठे-बैठे ही सुखबीर से कहा, "भाई, एक रुपया ले लो और एक लिहाफ दे दो. बड़ा भला होगा तुम्हारा." सुखबीर ने लिहाफ के ढेर की ओर निगाह घुमाई अभी भी चार बचे थे. सहसा ही उसे मालिक गनपत की हिदायत का ख़्याल हो आया कि चाहे कोई भी क्यों न हो, कोई छूट नहीं देनी है. उसने उसकी ओर मुखातिब होते हुए कहा, "कहा न, हमारे यहां एक ही रेट है, दो रुपए से कम नहीं." वह चुप हो गया. ठंडी हो गई लोई में ख़ुद को और अधिक समेटने का प्रयास करने लगा.
रात के दो बजे के लगभग अचानक सुखबीर की आंख खुल गई. थोड़ी देर पहले ही उसकी आंख लगी थी. बच्चे के रोने की आवाज़ उसके कानों में आने लगी. नींद की हड़बड़ाहट से जगे-जगे उसे एहसास हुआ, यह आवाज कहीं उसके अपने बच्चे के रोने की तो नहीं है. सहसा उसे ख़्याल आया यह तो उसकी खामख्याली है. वह तो इस वक़्त गांव में, घर के भीतर आराम से सो रहा होगा. उसने गर्दन घुमाकर देखा, पति-पत्नी जागे हुए बैठे थे और उनके बीच बच्चा लगातार रोए जा रहा था. अगल-बगल के लोग लिहाफों में घुसे हुए बेसुध सो रहे थे. वह पत्नी को डपट रहा था, "चुप करा इसे भागवान! सब लोगों की नींद ख़राब करेगा."
"क्या करूं, ठंड के मारे सो नहीं रहा है. कंबल तो जैसे पानी हो गया है." पत्नी गिडगिड़ाती सी बोली. वह चुप हो गया. कुछ नहीं बोला आगे.
सुखबीर कुछ क्षण न जाने क्या सोचता रहा, फिर झटके से उठा. ढेर में से दो लिहाफ उठाकर उन्हें दे आया. पत्नी ने झट से एक लिहाफ खींच लिया और बच्चे को लेकर उसमें दुबक गई.
"अब कुछ ही देर में तो दिन निकल आएगा. फिर किराया..?" उसने सुखबीर की ओर देखते हुए कहा.
"तेरा बच्चा, मेरा बच्चा है भाई. तुमसे किराया नहीं लूंगा. बस, एक मेहरबानी करना. सुबह मालिक के आने से पहले ही लिहाफ वापस कर देना." सुखबीर ने कहा और अपनी जगह वापस लौट आया. उसे अपने मालिक गनपत की हिदायत याद आने लगी. उसकी नींद गायब हो चुकी थी. उसे डर था कि कहीं सुबह ही सुबह मालिक न आ टपके. सुबह होने तक वह ऐसे ही बैठा रहा.
- शालिनी शर्मा

अधिक कहानियां/शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए यहां क्लिक करें – SHORT STORIES